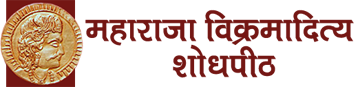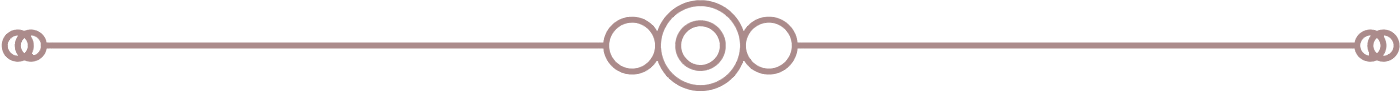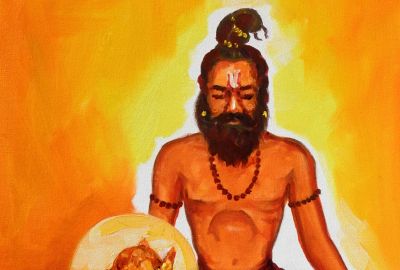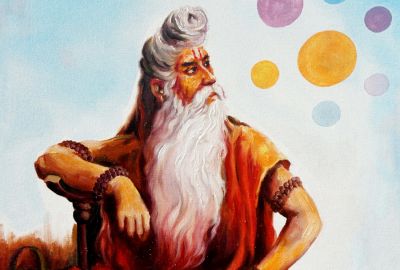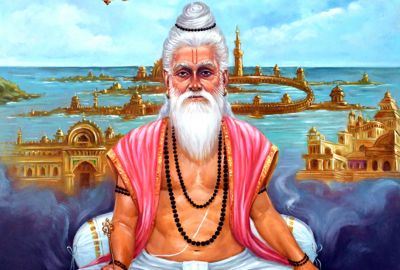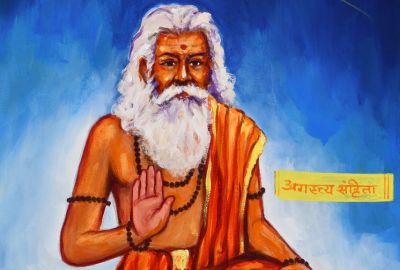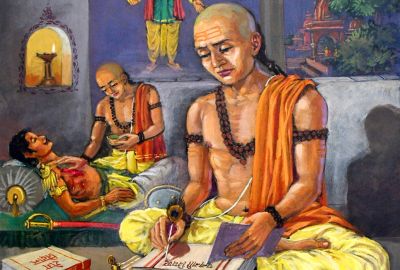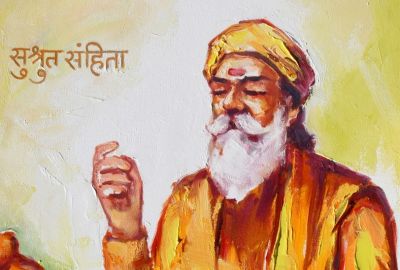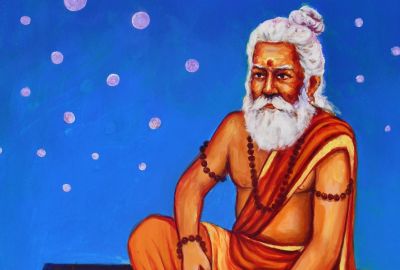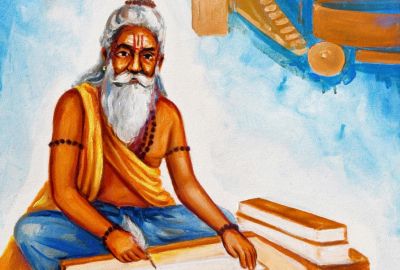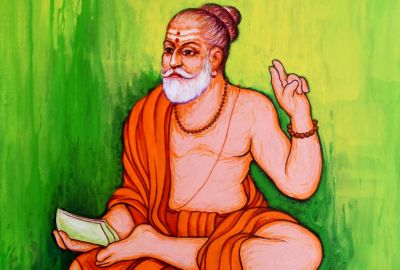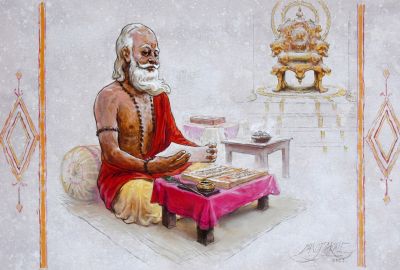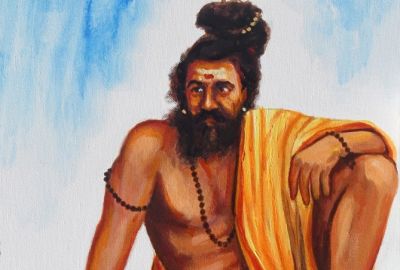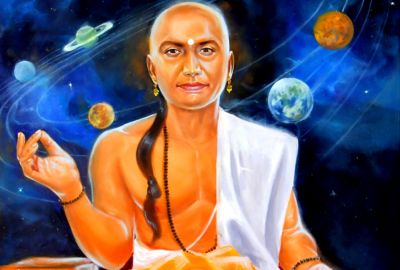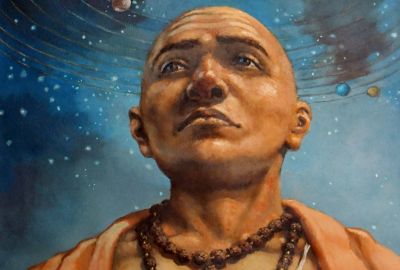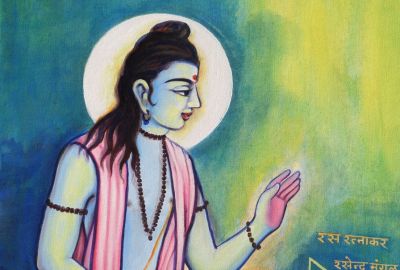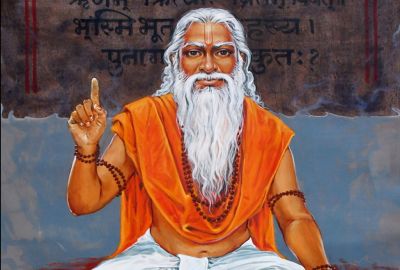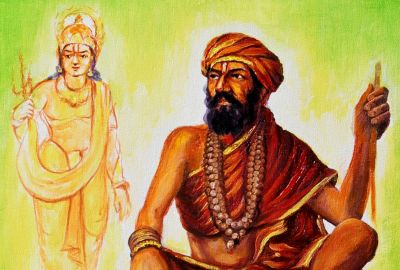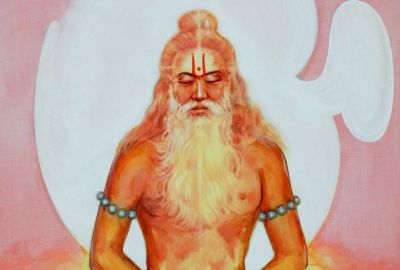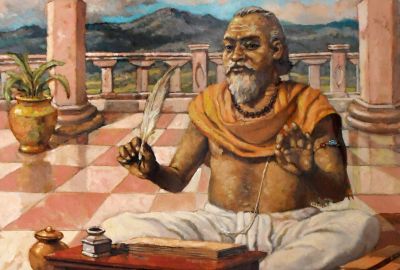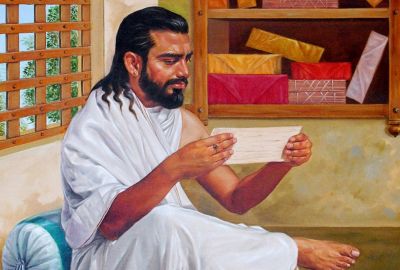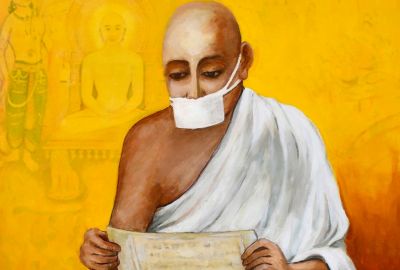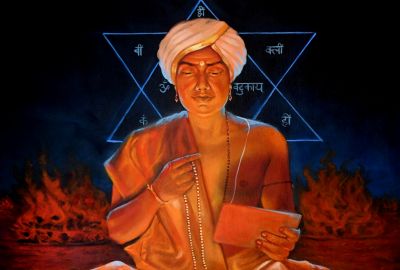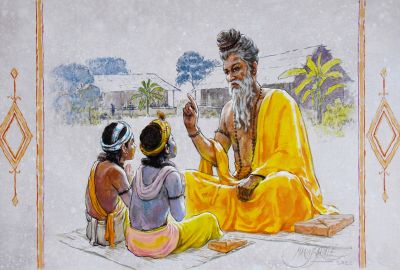गौतम
महाभारत के अध्ययन से विदित होता है कि गौतमीय न्याय दर्शन के सिद्धान्त उस समय के विद्वत्समाज में अधिक प्रचलित थे। महर्षि गौतम जिन्हें 'अक्षपाद गौतम' के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है, न्याय दर्शन के प्रथम प्रवक्ता माने जाते हैं। न्याय दर्शन का सूत्रबद्ध, व्यवस्थित रूप अक्षपाद के न्यायसूत्र में ही पहली बार मिलता है। महर्षि गौतम परम तपस्वी थे। महर्षि गौतम ने न्यायशास्त्र के अतिरिक्त स्मृतिकार भी थे तथा उनका धनुर्वेद पर भी ग्रंथ रचा था। गौतम के न्याय दर्शन के सोलह पदार्थ इस प्रकार हैं- प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। गौतम के न्यायसूत्र के पाँच अध्याय हैं। पहले अध्याय में गौतम ने सोलह पदार्थों की सूची देते हुए उनके लक्षण तथा कुछ स्थूल प्रकार दिये हैं। दूसरे अध्याय में गौतम ने संशय और प्रमाण की विशेष परीक्षा की है। तीसरे और चौथे अध्याय में प्रमेयों का विशेष विवेचन किया है। पाँचवें अध्याय में गौतम ने जाति और निग्रह स्थान का सविस्तार वर्गीकरण किया है। इससे मालूम होता है कि यद्यपि गौतम ने सोलह पदार्थों का लक्षण तथा वर्गीकरण किया है, तथापि प्रमाण, प्रमेय तथा संशय, इन तीन पदार्थों की उन्होंने विशेष परीक्षा की है। प्रमेयों का विवेचन गौतम ने बड़े विस्तार से किया है और यह करते समय समकालीन सत्ताशास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा भी गौतम ने की है।
गौतम के अनुसार प्रमाण, यथार्थ ज्ञान के चार साधन हैं- प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण वह शब्द प्रमाण। इन्द्रियों का विषय के साथ सम्बन्ध होने पर जो ज्ञान मिलता है, जो शब्दात्मक नहीं होता, तथा जो बाद में खंडित या बाधित न होने वाला निश्चयात्मक ज्ञान होता है, वही प्रत्यक्ष है। गौतम ने, प्रमा-यथार्थ अनुभव और प्रमाण, उस यथार्थ अनुभव का कारण याने साधन, इनमें अन्तर नहीं किया, इसीलिए उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कर दिया है। प्रत्यक्ष के बाद गौतम ने अनुमान का वर्णन किया है। गौतम मानते हैं कि अपवर्ग के लिए सर्वप्रथम मिथ्या ज्ञान का नाश होना चाहिए। इससे प्रतीत होता है कि न्यायविद्या चिरकाल से ही दृढ़मूल की तरह विशाल और वैविध्यपूर्ण रही है, जो वेद, पुराण, स्मृति तथा महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में विकीर्ण है। न्यायसूत्रकार महर्षि गौतम के समक्ष सुदृढ आधारशिला की तरह न्याय दर्शन के अनेक प्रसिद्ध सिद्धान्त उपलब्ध थे। इनमें से युक्तिसंगत सिद्धान्तों का चयन कर उसे शास्त्र रूप में प्रतिष्ठित करने के श्रेयस का लाभ इन्होंने किया। फलस्वरूप आज हम लोगों को पूर्णांग, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध न्यायदर्शन उपलब्ध है।